याद है तुम्हें ? उस रात को चांदनी में बैठकर कितने वादे किये थे कितनी कसमें खाईं थीं. सुना था, उस ठंडी सी हवा ने जताई भी थी अपनी असहमति हटा के शाल मेरे कन्धों से. पर मैंने भींच लिया था उसे अपने दोनों हाथों से. नहीं सुनना चाहती थी मैं कुछ भी किसी से भी. अब किससे करूँ शिकायत …

मन की राहों की दुश्वारियां निर्भर होती हैं उसकी अपनी ही दिशा पर और यह दिशाएं भी हम -तुम निर्धारित नहीं करते ये तो होती हैं संभावनाओं की गुलाम ये संभावनाएं भी बनती हैं स्वयं देख कर हालातों का रुख मुड़ जाती हैं दृष्टिगत राहों पे कुछ भी तो नहीं होता हमारे अपने हाथों में फिर क्यों कहते हैं कि आपकी जीवन रेखाएं …
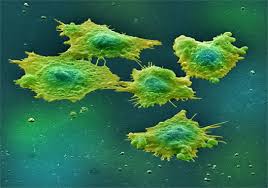
मैं नहीं चाहती लिखूं वो पल तैरते हैं जो आँखों के दरिया में थम गए हैं जो माथे पे पड़ी लकीरों के बीच लरजते हैं जो हर उठते रुकते कदम पर हाँ नहीं चाहती मैं उन्हें लिखना क्योंकि लिखने से पहले जीना होगा उन पलों को फिर से उखाड़ना होगा गड़े मुर्दों को कुरेदने होंगे कुछ पपड़ी जमे ज़ख्म और फिर उनकी दुर्गन्ध …

विशुद्ध साहित्य हमारा कुछ उस एलिट खेल की तरह हैजिसमें कुछ सुसज्जित लोग खेलते हैं अपने ही खेमे में बजाते हैं तालीएक दूसरे के लिए ही पीछे चलते हैं कुछ अर्दली थामे उनके खेल का सामान इस उम्मीद से शायद कि इन महानुभावों की बदौलत उन्हें भी मौका मिल जायेगा कभी एक – आध शॉट मारने का और वह कह सकेंगे हाँ वासी हैं वे भी उस तथाकथित पॉश दुनिया के जिसका — बाहरी दुनिया…








