कंपकपाते पत्ते पर
ठहरी एक बूँद ओ़स की
बचाए हुए किसी तरह
खुद को
तेज़ हवा उड़ा न दे
धूप कहीं सुखा न दे
उतरी है आकाश से
गिर न जाये धूल में
पर आखिर
मिलना पड़ता है उसे
उसी मिट्टी में
कंक्कड़ पत्थर के बीच ही
और वो लुप्त हो जाती है
उसी धूल मिटटी की धरा में
प्राणी भी तो
जन्म लेता है
लड़खड़ाते समाज की गोद में
फ़िर बचाता फिरता है
अपने अस्तित्व को,
अपनी पवित्रता को
इंसानियत को
इस संसारी थपेड़ों से
स्वार्थ की कड़ी धूप से
पर कब तक?
आखिर मिलना पड़ता है उसे भी
इसी जर्जर व्यवस्था में
बन जाता है वो भी
उनमें से ही एक
जो बनाते हैं
इस तथाकथित समाज को
जीना जो है उसे इसी परिवेश में.
ठहरी एक बूँद ओ़स की
बचाए हुए किसी तरह
खुद को
तेज़ हवा उड़ा न दे
धूप कहीं सुखा न दे
उतरी है आकाश से
गिर न जाये धूल में
पर आखिर
मिलना पड़ता है उसे
उसी मिट्टी में
कंक्कड़ पत्थर के बीच ही
और वो लुप्त हो जाती है
उसी धूल मिटटी की धरा में
प्राणी भी तो
जन्म लेता है
लड़खड़ाते समाज की गोद में
फ़िर बचाता फिरता है
अपने अस्तित्व को,
अपनी पवित्रता को
इंसानियत को
इस संसारी थपेड़ों से
स्वार्थ की कड़ी धूप से
पर कब तक?
आखिर मिलना पड़ता है उसे भी
इसी जर्जर व्यवस्था में
बन जाता है वो भी
उनमें से ही एक
जो बनाते हैं
इस तथाकथित समाज को
जीना जो है उसे इसी परिवेश में.


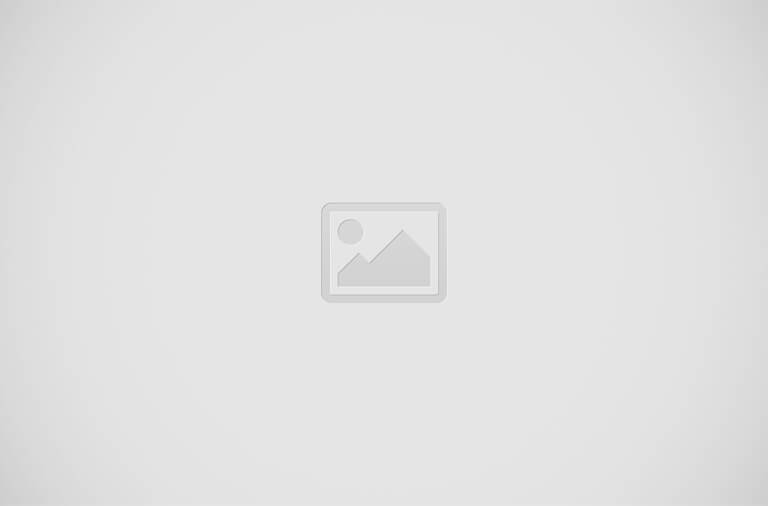
हिंदी ब्लॉग की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है…
अच्छी शुरुआत है,जारी रखें
http://gazalkbahane.blogspot.com/
कम से कम दो गज़ल [वज्न सहित] हर सप्ताह
http:/katha-kavita.blogspot.com/
दो छंद मुक्त कविता हर सप्ताह कभी-कभी लघु-कथा या कथा का छौंक भी मिलेगा
सस्नेह
श्यामसखा‘श्याम
word verification हटाएं
vah vah………bahut achhi rachna
BADHAI HO
जीवन की सार्थकता को ओस की बूंदों के माध्यम से …………लाजवाब रूप मेकं कहा है आपने
स्वागत है आपका ब्लॉग जगत में
व्यापक तुलना आपकी पढ़ा तो आया होश।
शीर्षक में ओअस लिखा लिख दें उसको ओस।।
सादर
श्यामल सुमन
09955373288
http://www.manoramsuman.blogspot.com
shyamalsuman@gmail.com
अच्छा प्रयास
शुभकामनायें
yaar baniye kab se itna achha likhne lage……
great poetry shikha…like it, something of my taste. keep it up
Sundar shuruaat hai..anek shubhkamnayen…
sneh
shama
संघर्ष की शुरूआत का इतना मजबूर अंत..उफ़..
शुभकामनाएं…
उसी मिटटी में
कंक्कड़ पत्थर के बीच ही
और वो लुप्त हो जाती है
उसी धूल मिटटी की धरा में
प्राणी भी तोजन्म लेता है
bhot hi sundar khyaal….umda
rqt…apne blog par ek lock lagale jis se koi kavita ya gazal chori naa kar sake.
thnxx..meri gazal bhi pade.
http://www.bedildeepak.tk
आप की रचना प्रशंसा के योग्य है . लिखते रहिये
चिटठा जगत मैं आप का स्वागत है
गार्गी
kya baat hai
yakeen nahi hota
itne gahre bhaav samete huye kavita kaise likhi aapne ?
bahut achhi kavita hai.
meri hardik shubhkamnayen
बहुत सुंदर…..आपके इस सुंदर से चिटठे के साथ आपका ब्लाग जगत में स्वागत है…..आशा है , आप अपनी प्रतिभा से हिन्दी चिटठा जगत को समृद्ध करने और हिन्दी पाठको को ज्ञान बांटने के साथ साथ खुद भी सफलता प्राप्त करेंगे …..हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बहुत सुंदर
शुभकामनाएं
http://www.ashokvichar.blogspot.com
nice one. narayan narayan
बिलकुल सही बात कही है।
सादर
वाह !
सुंदर रचना …
बधाई !!
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति ।
बहुत सुन्दर भाव …
सच बात कही……..
सार्थक रचना..
सुन्दर भावों से युक्त रचना.
hello!,I like your writing very a lot! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.
Really clean internet site, thanks for this post.